हिंदी भाषाचिंतन को प्रो. दिलीप सिंह का अवदान
-ऋषभदेव शर्मा
हिंदी भाषाविज्ञान की परिवर्तनशील प्रकृति और उसके व्यापक होते जा रहे सरोकारों पर जिन इने-गिने भाषा अध्येताओं का ध्यान गया है उनमें प्रो. दिलीप सिंह (1951) का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने भाषावैज्ञानिक चिंतन को नवीन भाषा संदर्भों में परखने और तदनुरूप निष्पत्तियाँ प्रतिपादित करने का चुनौतीपूर्ण दायित्व निभाया है। उन्होंने अपने लेखन द्वारा भाषावैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर केंद्रित भाषा संदर्भ को सुनिश्चित समृद्धि प्रदान की है। वे एक ऐसे मर्मवेधी भाषावैज्ञानिक-समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिसकी दृष्टि सदा सकारात्मक, वस्तुनिष्ठ तथा कृतिकेंद्रित रहती है। वे साहित्य और भाषा को संस्कृति की ऐसी निष्पत्ति मानते हैं जिसका लक्ष्य मनुष्य और उसकी सामाजिकता है क्योंकि उनके लिए साहित्य और भाषा का विश्लेषण वस्तुतः मानव जीवन को सुंदरतर और समृद्धतर बनाने की साधना का ही दूसरा नाम है। उनकी यह मान्यता केवल लेखन तक सीमित नहीं है बल्कि उनका व्यक्तित्व भी इसी के ताने-बाने से बुना हुआ प्रतीत होता है। भाषा, समाज, संस्कृति और साहित्य इन चारों को आंतरिक रूप से संबंधित और परस्पर आश्रित मानने वाले प्रो. दिलीप सिंह अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक आचरण में भी इन चारों के समीकरण को चरितार्थ करने वाले आधुनिक भाषाचिंतक हैं। वे बौद्धिक जड़ता को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करते और समय की माँग के अनुरूप हर परिस्थिति में कुछ नया करने के लिए तत्पर रहते हैं।
समाज को भाषा का नियामक मानने वाले प्रो. दिलीप सिंह व्यक्त वाणी के साथ ही देह भाषा और संकेतों में निहित संस्कृति के भी गहन पारखी और प्रयोक्ता हैं। आँखों में अजीब आत्मीयताभरी चमक, मूँछों में रहस्यपूर्ण स्मित और होठों पर निश्छल अट्टहास उनके धीर-गंभीर व्यक्तित्व को रुक्ष होने से बचाते हैं। सामान्य वार्तालाप में विनम्रता और शालीनता का प्रतिपल ध्यान रखने वाले प्रो. दिलीप सिंह वक्ता के रूप में अत्यंत ओजस्वी और दृढ़ संप्रेषक माने जाते हैं जो प्रमाणों और उदाहरणों के बिना कभी नहीं बोलते और किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले विषय की आंतरिक तहों का अलग-अलग कोणों से खुलासा करते हैं। उनका लेखकीय व्यक्तित्व शोधकर्ता और सर्जक के अद्भुत सामंजस्य से निर्मित है।
प्रो. दिलीप सिंह ने भाषाचिंतन की दीक्षा प्रो. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव और पंडित विद्यानिवास मिश्र सरीखे भाषाविदों से प्राप्त की। उनकी भाषावैज्ञानिक मेधा वाराणसी, आगरा, धारवाड़, हैदराबाद और मद्रास जैसे भारत के अलग-अलग भाषिक स्वभाव वाले केंद्रों में शाणित हुई तथा फ्रांस और अमेरिका की भट्टियों में तपकर निखरी। ‘समसामयिक हिंदी कविता’ (1981) और ‘व्यावसायिक हिंदी’ (1983) जैसी क्रमशः संपादित और मौलिक पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने आरंभ में ही यह संकेत दे दिया था कि वे साहित्य अध्ययन और भाषाविज्ञान को परस्पर निरपेक्ष अनुशासन नहीं मानते। काव्य-भाषा और काव्य-शैली की भी उनकी समझ उतनी ही निर्मल हैं जितनी प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद चिंतन की। आगे बढ़ने से पहले यह और जान लेना आवश्यक है कि प्रो. सिंह ने साहित्य और भाषा क्षेत्र के विशिष्ट और वरिष्ठ विद्वानों के साथ मिलकर प्रो. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव की हिंदी और अंग्रेज़ी में रचित संपूर्ण ग्रंथावली का संपादन किया है तथा विविध विश्वविद्यालयों और संस्थानों के भाषाविज्ञान के पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री भी विकसित, संपादित और प्रकाशित की है। इन सारे ही कामों में उनकी समाजभाषिक चेतना को प्रतिफलित देखा जा सकता है। वे संप्रेषण पर सर्वाधिक बल देनेवाले व्यावहारिक भाषाविज्ञानी हैं, इसमें संदेह नहीं। अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के व्यावहारिक प्रयोक्ता भाषाचिंतक के रूप में प्रो. दिलीप सिंह की ख्याति का आधार बनने वाले उनके ग्रंथों में ‘भाषा, साहित्य और संस्कृति’ (2007), ‘पाठ विश्लेषण’ (2007), ‘भाषा का संसार’ (2008), ‘हिंदी भाषाचिंतन’ (2009), ‘अन्य भाषा शिक्षण के बृहत संदर्भ’ (2010), ‘अनुवाद की व्यापक संकल्पना’ (2011) और ‘कविता पाठ विमर्श’ (2013) जैसी कृतियाँ शामिल हैं।
प्रो. दिलीप सिंह के इस समस्त भाषावैज्ञानिक लेखन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने साहित्य विमर्श और भाषाचिंतन दोनों ही दृष्टियों से हिंदी जगत को समृद्ध किया है। एक ओर उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के पाठों के मर्म का भेदन करके उनके सौंदर्य का उद्घाटन किया है तथा दूसरी ओर सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के विविध पक्षों को व्यवहारतः घटित करके दिखाया है। उनका समस्त चिंतन भारतीय मनीषा की परंपरानुसार भाषाकेंद्रित चिंतन है तथा अपने लेखन द्वारा उन्होंने इस परंपरा को आधुनिक दृष्टि से भी संपन्नतर बनाने का महत्कार्य किया है।
सामान्यतः आज भी यह माना जाता है कि भाषाविज्ञान जटिल वैचारिकता का शास्त्र है। लोग यह भी सोचते हैं कि भाषाविज्ञान सैद्धांतिकी में बुरी तरह जकड़ा हुआ एक ऐसा तथ्यपरक अध्ययनक्षेत्र है जिसका आदि ही उसका अंत होता है। परंतु पिछले पाँच दशकों में भाषाविज्ञान अथवा भाषावैज्ञानिक अध्ययन की प्रविधियों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। एक ओर भाषा विवरण की सरणियाँ अर्थकेंद्रित हुईं तो दूसरी ओर अर्थ की सीमाएँ, जो परंपरागत भाषाविज्ञान में बोध तक सीमित थीं, प्रैगमेटिक्स तक फैल गईं। फिर भाषावैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर जो विमर्श हुए उन्होंने इस धारणा को तो कमज़ोर किया ही कि भाषाविज्ञान सिर्फ भाषा सिद्धांत अथवा भाषा विवरण की संरचनात्मक बुनावट को खोलने वाला शास्त्र है, यह भी प्रतिपादित किया कि वह अनुप्रयोग की जा सकने वाली एक उपयोगी प्रणाली भी है। इसी संदर्भ में प्रो. दिलीप सिंह ने भाषा सैद्धांतिकी और इसके अनुप्रयोग की सभी दिशाओं को टटोला और अपनी अवधारणाएँ प्रकट कीं। उनका लेखन भाषावैज्ञानिक चिंतन की संप्रेषणीयता का हामी है। सिद्धांतों को वे अपने भीतर जिलाते हैं और फिर उन्हें अनुप्रयोगात्मक स्तर पर भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज के घटकों के भीतर से प्रतिफलित करने का यत्न करते हैं। भाषावैज्ञानिक चिंतन में उनका अवदान यह माना जाएगा कि समय-समय पर उद्घाटित भाषिक और भाषावैज्ञानिक लेखन की अवधारणाओं को उन्होंने डाटा, पाठ और व्यावहारिक भाषा सामग्री के सहारे प्रस्तुत किया है। उनके भाषावैज्ञानिक लेखन का विस्तृत क्षेत्र ही यह जताने के लिए काफी है कि उनकी अध्ययन पीठिका कितनी मजबूत, तर्कबद्ध और पारदर्शी है। दूसरे शब्दों में उनका अवदान उनके सुदीर्घ चिंतन-मनन का निचोड़ है।
समाजभाषाविज्ञान
प्रो. दिलीप सिंह ने पिछली शताब्दी के सातवें दशक में ‘सामाजिक स्तर भेद और भाषा स्तर भेद’ विषय पर पीएचडी की थी। यह वह समय था जब भारत में भाषावैज्ञानिक विमर्श में समाजभाषाविज्ञान घुटनों के बल चल रहा था। दिलीप सिंह ने समाजभाषावैज्ञानिक सिद्धांतों को हिंदी भाषासमुदाय के भाषा वैविध्य के नज़रिए से विश्लेषित किया जिसमें यह अछूता पक्ष भी उजागर किया कि सामाजिक संरचना ही भाषा वैविध्य और भाषा विकास को संभव बनाती है। आगे चलकर समाजभाषाविज्ञान उनके लेखन का एक मूलाधार भी बना। उन्होंने पहली बार ‘समाजभाषाविज्ञान’ और ‘भाषा का समाजशास्त्र’ की वैचारिकता को ही स्पष्ट नहीं किया बल्कि ‘भाषा का समाजशास्त्र’ की सैद्धांतिकी में उल्लिखित उन सभी पक्षों को हिंदी भाषा के संदर्भ में व्याख्यायित किया जिनका उस समय तक तो अभाव था ही, आज भी जितना विस्तार इसे हिंदी भाषा की भाषिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक छवियों के संदर्भ में मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका है। प्रो. सिंह निरंतर इस दिशा में विचार करते आ रहे हैं। चाहे वे साहित्यिक पाठों का विश्लेषण कर रहे हों, चाहे हिंदी प्रयुक्तियों की व्याख्या, और चाहे अनुवाद प्रक्रिया और अन्य भाषा शिक्षण - सभी में एक संकेत की तरह वे समाजभाषावैज्ञानिक और भाषा की समाजशास्त्रीय प्रविधियों का निर्माण और प्रयोग करने की पहल करते हैं।
इस दृष्टि से उन्होंने विकल्पन, संप्रेषण और भाषा की सर्जनात्मकता पर जो चर्चाएँ की हैं, वे भारतीय भाषाओं और खासकर हिंदी भाषा के लिए आधार बनाई जा सकती हैं। प्रो. सिंह ने समाजभाषाविज्ञान की अपनी अध्ययन दृष्टि को बहुत व्यापक बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें सस्यूर और चाम्स्की के वैचारिक द्वंद्वों से भी वे टकराए हैं ; लेबाव और हैलीडे की व्यावहारिकता को भी उन्होंने नए ढंग से देखा है तथा डेल हाइम्स के बहाने भाषा में संस्कृति के अंतस्थ होने की अनिवार्यता का भी पता उन्होंने दिया है। प्रयोग, संदर्भ, परिस्थिति और संप्रेषण जैसी सैद्धांतिक संकल्पनाओं को प्रो. सिंह ने हिंदी भाषा और साहित्य के विवेचन द्वारा जिस तरह पठनीय, संप्रेषणीय और वैज्ञानिक रूप में सामने रखा है वह उनके प्रवीण समाजभाषावैज्ञानिक होने का स्वतः प्रमाण है।
शैलीविज्ञान
इसमें संदेह नहीं कि शैलीविज्ञान की जिन अवधारणाओं से प्रो. दिलीप सिंह प्रभावित दिखाई देते हैं, वह रवींद्रनाथ श्रीवास्तव का शैलीवैज्ञानिक चिंतन है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रीवास्तव का चिंतन एक जटिल वैचारिक प्रक्रिया से उद्बुद्ध है अतः उसे ठीक ढंग से समझना, उसके भीतरी बिंदुओं की पहचान करना और फिर उन्हें पाठ के संदर्भ में उपयोग में लाना आसान काम नहीं है। इस बात से ही पता चलता है कि वे शैलीविज्ञान के गहन अध्येता हैं और यह भी कि श्रीवास्तव में उद्धृत अन्य संदर्भों को उन्होंने अलग से भी पढ़ा-समझा और फिर अपनी एक राह बनाई। प्रो. सिंह ने भाषा, समाज और साहित्य को अविच्छिन्न देखा है। उनकी साहित्यिक अभिरुचि पाठ के भाषिक विधान से तय होती दिखाई देती है। संस्कृति संबंधी उनकी धारणाएँ भी रीति-रिवाज और आचरण से आगे जाकर प्रोक्ति में इनको घटित होते हुए देखती हैं। उनका समाजभाषावैज्ञानिक पक्ष भी प्रबल है क्योंकि यहाँ भी उन्होंने सामाजिक शैली, शैली वैविध्य, पाठों में गठाव और भाषिक अभिव्यंजना को मात्र चयन, विचलन, समांतरता और अग्रप्रस्तुति के खाँचों में न बाँट कर पाठ में द्वंद्व या तनाव तथा अभिव्यंजनात्मक औज़ारों के नजरिये से शैली की सहजता को आँकने की कोशिश की है। शैलीविज्ञान में इनका अवदान यह माना जा सकता है कि शैलीविज्ञान को शुद्ध भाषाई और संरचनात्मक मानने वाली विचारधारा को उन्होंने चुनौती दी और विभिन्न पाठों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि शैलीविज्ञान साहित्यिक पाठ के विश्लेषण की ऐसी प्रविधि है जो सामाजिक शैलीविज्ञान तक जाने का रास्ता भी हमें दिखलाती है। उनका अवदान यह भी है कि वे शैलीविज्ञान को समाजशैलीविज्ञान के दायरे में ले जाते हैं और हिंदी के पाठों के जरिये यह दिखा पाते हैं कि शैलीविज्ञान केवल भाषिक संरचना पर केंद्रित न होकर कला, संस्कृति और सभ्यता के विकास से भी साहित्य को जोड़ने का मार्ग दिखाता है।
प्रो. सिंह ने शैली की अवधारणा को भी नए आयाम दिए। सामाजिक शैली, बातचीत में लोक और सांस्कृतिक तत्वों का अवमिश्रण, संवादों की परिस्थितिजन्य बुनावट तथा प्रोक्ति के स्तर पर पाठों की अभिव्यंजनापरक संघटना को वे इस दृष्टि से देखते हैं कि यह स्पष्ट हो सके कि कृति के भीतर सन्निहित शैलीतत्व अपनी विविधता तो प्रकट करते ही हैं, वे कृति की आत्मा और मार्मिकता को भी उभार दे सकते हैं, देते हैं।
प्रो. सिंह ने अपने शैलीवैज्ञानिक अनुप्रयोगों में एक उल्लेखनीय काम यह भी किया है कि उन्होंने हिंदी की व्याकरणिक इकाइयों के सृजनात्मक प्रयोग की पड़ताल गद्य और पद्य दोनों प्रकार के पाठों मंे की है। इसके पहले पाठ विष्लेषण में इस प्रविधि का उपयोग दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त भाषा और संवेदना के नजरिए से भी प्रो. सिंह ने कभी षिल्प तो कभी पाठों की संरचना के द्वारा यह उद्घाटित किया है कि भाव और संवेदना को अपेक्षित उत्कर्ष देने में भाषिक विधान तथा भाषायी संयोजन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने शैलीविज्ञान को व्यावहारिकता में ढालकर यह जता देने का यत्न किया है कि मात्र सैद्धांतिकता किसी शाास्त्र का न तो मूल होती है और न ही उसकी अंतिम परिणाति। जब तक उसका अनुप्रयोग नहीं किया जाता और सही प्रविधि से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक उसके प्रति भ्रांतियाँ बने रहने की तथा निरर्थक बहस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शैलीविज्ञान की पृष्ठभूमि अत्यंत ठोस है तथा हिंदी के साहित्यिक पाठों की सटीक समीक्षा में इसे किस तरह अपनाया और पनपाया जा सकता है यह उनके पाठ विष्लेषण से समझने में हमें कोई दिक्कत पेष नहीं आती। एक विषेषता यह भी कि शैलीविज्ञान के सिद्धांतों को उन्होंने अपने भीतर पचाया है और फिर पाठों के जरिये उन्हें रूपाकार दिया है। इसीलिए उनके इन अध्ययनों में हमें न तो कोई झोल दिखाई देता है, न अस्पष्टता और न ही भ्रांति। संप्रेषणीयता उनके इस लेखन का अतिरिक्त गुण है जो ऐसे लेखनों में कदाचित ही दीख पड़ता है।
(अन्य) भाषा शिक्षण
यह जानकारी हो सकती है कि प्रो. सिंह ने अपने कैरियर की शुरूआत पहले विदेश और फिर देश में हिंदी शिक्षण से की। विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का उनका सुदीर्घ अनुभव रहा है। साथ ही दक्षिण भारत में बरसों हिंदी पाठ्यक्रमों से और शोध से जुड़े होने के कारण उनकी दृष्टि भाषा अधिगम की उन समस्याओं पर स्वतः पड़ती रही है जिनकी वजह से दूसरी भाषा के ग्रहण में अथवा समझ में व्यवधान उत्पन्न होता है। अपने इन्हीं अनुभवों को प्रो. सिंह ने भाषा शिक्षण संबंधी लेखन में हमारे साथ बाँटा है। यहाँ भी व्यावहारिकता का दामन उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा है। इसके पहले उनके सामने हिंदी में भाषाविज्ञान और भाषा शिक्षण, लेंगुएज टीचिंग एंड स्टाइलिस्टिक्स और व्यतिरेकी विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली अनेक पुस्तकें थीं। इनमें से अधिकतर सैद्धांतिक ज्यादा थीं, व्यावहारिक कम। उन्होंने एक काम महत्वपूर्ण किया; और जिसका अनुभव वे विदेश में कर चुके थे कि मसला केवल भाषा शिक्षण भर का नहीं है इसकी परिधि में साहित्य और संस्कृति शिक्षण का भी समावेश होना चाहिए। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। भाषाशिक्षण की बात करते समय प्रो. दिलीप सिंह ने पहली बार उसकी ऐतिहासिकता को ही नहीं बल्कि इतिहास के माध्यम से उसकी विकास प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश की क्योंकि इन्हें समझे बिना उन समस्याओं को समझ पाना भी कठिन है जो भाषा अधिगम में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस संदर्भ में पुनः उनका जोर संप्रेषणपरक भाषा शिक्षण पर है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसे उन्होंने ‘अभिव्यक्ति की व्यवस्था’ कहा और इस अभिव्यक्ति की व्यवस्था में उन्होंने भाषिक के साथ-साथ भाषेतर उपादानों को अन्य भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अनिवार्य सिद्ध किया है, ऐसा हिंदी में पहली बार घटित हुआ। इसके साथ ही अन्य भाषा शिक्षण में लिखित और उच्चरित भाषा के बीच भेदों और अंतर्संबंधों दोनों को लेकर चलने की जो प्रविधियाँ उन्होंने तैयार की हैं, वे अनूठी तो हैं ही, भाषिक सामग्री का उपयोग करने की वजह से ये कक्षा में उपयोग करने योग्य भी बन गई हैं। इस धरातल पर ही रूप के स्थान पर अर्थ पर बल देने तथा भाषा के प्रकार्यात्मक रूपों को अधिक स्थान देने की जो बात उन्होंने कही है वह संप्रेषण से भी आगे जाकर अन्य भाषा में बोधगम्यता और दक्षता तक पहुँचती है। इसीलिए भाषा दक्षता को प्रो सिंह ने अलग नजरिये से देखा है। तभी उन्होंने संप्रेषण सिद्धांत के अंतर्गत रोमन याकोब्सन और हैलीडे के विचारों को इतना उदाहरणपुष्ट और पारदर्शी बना दिया है जैसा कि कर पाना किसी सामान्य के बूते का नहीं है।
साहित्य शिक्षण (अभी तक जिस पर हिंदी में कोई चर्चा ही नहीं हो पाई है) की उनकी स्थापनाएँ अनुभवसिद्ध हैं। साहित्यिक पाठों में भाषा शिक्षण के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा समाजमनोवैज्ञानिक घटकों को कैसे शिक्षणीय बनाया जा सकता है, यह प्रो. सिंह ने प्रक्रियात्मक पद्धति अपनाते हुए समझाया है। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि साहित्यिक पाठ के जो अंश उन्होंने साहित्य शिक्षण की बात करते हुए उदाहरणस्वरूप चुने हैं, वे वहीं से उठाए गए हैं जिन्हें वे पाठ विश्लेषण के लिए पहले चुन चुके थे। इस तरह उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि पाठ विश्लेषण की परिधि में वे जिन शैलीवैज्ञानिक प्रविधियों का इस्तेमाल कर रहे थे वे बड़ी आसानी से भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ उनका शैलीवैज्ञानिक और समाजभाषावैज्ञानिक दोनों मुखर हैं।
संस्कृति शिक्षण पर उनका लेखन पहली बार दिखाई दिया है जिसके माध्यम से उन्होंने यह प्रतिपादित करने का यत्न किया है कि भाषा और संस्कृति का संबंध बेजोड़ होता है तथा पहली बार यह भी कि सांस्कृतिक तत्वों के घुलन के बिना न तो किसी सामाजिक भाषा का निर्माण होता है और न ही किसी सभ्यता का।
इस क्षेत्र में प्रो. सिंह ने भाषा शिक्षण की सैद्धांतिकी को भी प्रस्तुत किया है। इस सैद्धांतिक भूमिका को उन्होंने निःसंकोच प्रो. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव से ग्रहण कर लिया है और जहाँ जरूरत पड़ी है उसमें अपना कुछ जोड़ा है। जोड़ना और आगे की दिशा तय करना अथवा एक चिंतनबिंदु से दूसरे-तीसरे तक पहुँचना, प्रो. सिंह की भाषावैज्ञानिक लेखन पद्धति की अनोखी विशेषता है जिसे न तो दुहराव ही कहा जा सकता है और न ही पिष्टपेषण। उन्होंने भाषा षिक्षण के अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान से जुड़ने की या उसका अंग होने की चर्चा में अपनी इसी प्रतिभा का परिचय दिया है। जहाँ अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान को सैद्धांतिक भाषाविज्ञान के अनुप्रयोग तक सीमित न करके उन्होंने शुद्ध भाषाविज्ञान, समाजभाषाविज्ञान, मनोभाषाविज्ञान और यहाँ तक कि अनुवाद शास्त्र को भी इस तरह इसमें समाहित कर दिया है कि भाषा शिक्षण की जिन प्रविधियों को वे व्यावहारिक स्वरूप देते हैं वे यहाँ अपनी सैद्धांतिकता में भी दृढ़ बनी दिखाई देती हैं।
भाषा शिक्षण की अधुनातन आवश्यकताओं की ओर भी उनकी दृष्टि बराबर रही है। संप्रेषणपरक व्याकरण को तो वे वरीयता देते ही हैं लेकिन इसके भीतर वे सिर्फ बोलचाल की हिंदी या बातचीत की हिंदी की दक्षता तक ही इसकी सफल परिणति नहीं मानते हैं। उन्होंने पहली बार संप्रेषणपरक व्याकरण के भीतर अखबारों, फिल्मों, टीवी, रेडियो, लोक कलाओं, विशेष रूप से नाटकों के पाठों और भाषाविधान को भी अन्य भाषा शिक्षण में समाविष्ट करने का आग्रह किया है। इसीलिए विदेशी भाषा शिक्षण में विशेष रूप से उन्होंने ‘मीडिया और हिंदी’ पर अलग से बात की है और अन्य भाषा शिक्षण प्रकार्य को ‘लेंगुएज एफीशिएंसी’ की दृष्टि से प्रबल बनाने के लिए कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण पर भी उनके विचार अत्यंत वैज्ञानिक और सामग्रीपुष्ट हैं। यह भी शिक्षणीय है और यही उनकी चरम उपलब्धि भी है। जैसा कि उनसे अपेक्षित भी था, अन्य भाषा शिक्षण के समाजभाषिक पक्ष पर उन्होंने अलग से और विस्तार से विचार किया है। और एक अनूठा प्रयोग भी कि ‘तराना-ए-हिंदी’ के माध्यम से भाषाई तनाव और राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने वाली भाषिक संरचना को उन्होंने भाषा शिक्षण की दृष्टि से संप्रेषित किया है। एक विषेष बात यह भी है कि भाषा शिक्षण पर उनके चिंतन में व्यावहारिकता अथवा इन्हें कक्षा में इस्तेमाल कर पाने की सहजता तो निहित है ही, इनमें ऐसे अनेक प्रारूप हैं जिनका सीधा उपयोग करके अन्य भाषा शिक्षण के मार्ग को, और अन्य भाषा शिक्षार्थी को भी, अधिक दक्ष, समर्थ और सक्षम बनाया जा सकता है। उनके भाषा शिक्षण संबंधी लेखन का यह सबसे बड़ा अवदान है।
अनुवाद विज्ञान
अनुवाद संबंधी अध्ययन भी प्रो. दिलीप सिंह का प्रमुख क्षेत्र है। इसकी वजह अनुवाद की व्यावसायिकता अथवा अनुवाद पाठ्यक्रमों की अधिकता नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कि उनको शैलीविज्ञान, समाजभाषाविज्ञान और भाषा शिक्षण इन तीनों को जोड़ते हुए देखने का एक रास्ता इस चिंतन में सुझाई देता है। वे अनुवाद विज्ञान की परिपाटीगत व्याख्या में एकदम प्रवेश नहीं करते। न तो वे अनुवाद प्रकारों पर बीसियों पृष्ठ खर्च करते हैं, न ही उसकी प्रक्रिया पर और न ही उसकी उन घिसी पिटी परिभाषाओं पर जिनका अब न तो कोई ओर रह गया है न छोर। उनकी दृष्टि केवल सिद्धांत और समस्याओं पर भी टिकी नहीं है और अगर कहीं टिकी भी है तो पूरी नव्यता के साथ और अनुवाद को उस तरह देखने की अनिवार्यता के साथ कि अनुवाद एक शास्त्र और एक क्रिया की तरह आधुनिक समाज ही नहीं बल्कि वैश्विक समाज को किस रूप में आगे ले जा सकता है अथवा जोड़ सकता है। इसी कारण वे अपनी बात को प्राकृतिक अनुवाद से शुरू करते हैं जिसे एकभाषी भी अंजाम देता है। उन्होंने पहली बार यह बताया कि कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रिया द्विभाषी ही नहीं होती, एकभाषी भी होती है। इस संदर्भ में उन्होंने अनूदित पाठ का जो सिद्धांत दिया है वह एक ओर उनकी समाजभाषावैज्ञानिक दृष्टि के प्रस्थान को प्रतिबिंबित करता है तो दूसरी ओर उनकी शैलीवैज्ञानिक प्रविधियों की पकड़ को। ऐसा इसलिए कि इस नई भूमिका को स्थापित करते समय वे जिन दो संकल्पनाओं को आधार बनाते हैं वे हैं पाठभाषाविज्ञान और संकेतविज्ञान। अनुवाद चर्चा में यह दृष्टि अन्यत्र सुलभ नहीं है। शायद इसीलिए वे अनुवाद के सामाजिक संदर्भ को भी उभार सके हैं जिसे उनकी नव्यता निःसंकोच होकर कहा जा सकता है।
उनके अनुवाद चिंतन में तीन बातें बहुत खुलकर और पहली बार आई हैं -एक अनुवाद समीक्षा और मूल्यांकन वाला पक्ष, दो - तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद के अंतःसंबंध और इनकी अन्योन्याश्रयता का संदर्भ तथा तीन - साहित्येतर अनुवाद का संदर्भ। कहना न होगा कि प्रो. सिंह के पहले इन तीनों पर विचार तो क्या संकेत भी नहीं मिलते।
समतुल्यता के सिद्धांत को उन्होंने संप्रेषणपरक मूल्यों से भी और भाषाविकल्पन से जोड़कर अनुवाद को मात्र एक भाषिक रूपांतरण न मानकर एक समाजसांस्कृतिक रूपांतरण प्रक्रिया सिद्ध कर दिया है। इन चर्चाओं में भी वे अपनी व्यावहारिकता कायम किए हुए हैं जिसे वे मूल और अनूदित पाठों की तुलनीयता के द्वारा सिद्ध करते हैं। नाइडा के समतुल्यता सिद्धांत को प्रो. सिंह ने अलग ढंग से विवेचित किया है जिसमें रूपात्मक समतुल्यता और गत्यात्मक समतुल्यता को उन्होंने हिंदी पाठ के संदर्भ में देखा है और यहाँ भी भाषिक उपादानों से अधिक महत्व उन्होंने सामाजिक अर्थ को दिया है। संभवतः इसीलिए अनुवाद समस्या को भी वे एक नए नजरिये से देख सके हैं। यहाँ उनका बल भाषावैज्ञानिक समीक्षा से अधिक अर्थ, भाषेतर संदर्भ, विशिष्ट प्रयोग, सांस्कृतिक रूपांतरण और भाषा प्रकार्य संबंधी समस्याओं तक फैलता चला गया है। इसमें क्या संदेह है कि साहित्यिक और साहित्येतर दोनों प्रकार के पाठों में ये तमाम तरह की समस्याएँ उभरती रहती हैं। फिर भी इस पर हमें कोई चर्चा दिखाई नहीं देती। ऐसा करके प्रो.सिंह ने अनुवाद कार्य को रूपांतरण के एक तरीके से कहीं आगे ले जाकर भाषाविकास की एक प्रक्रिया माना है। कहना न होगा कि इसके पहले भाषा विकास के संदर्भ में अनुवाद की भूमिका को अथवा उसके देय को नज़रअंदाज कर दिया गया था।
हिंदी में पहली बार अनुवाद समीक्षा और मूल्यांकन को प्रो. सिंह ने तरजीह दी। यहाँ भी उन्होंने तब तक उपलब्ध इस संकल्पना पर प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तकों और एकाध हिंदी पुस्तक की सैद्धांतिकी से किनारा करते हुए अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी पाठों की समीक्षा के प्रारूप तैयार किए। उल्लेखनीय यह भी है कि उनके इस प्रारूप में कहीं ओट में हिंदी भाषा का इतिहास भी झाँकता है तो कहीं अंग्रेजी भाषासमाज की दुनिया को देखने वाली सीमित मानसिकता भी। ‘अनूदित पाठ में संप्रेषणीयता’ अथवा ‘अनूदित पाठ की संप्रेषणीयता’ यहाँ भी उनके लिए सर्वोपरि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा शैली में अनुवादनीयता की परख संभवतः उन्होंने पहली बार की और इसी तरह ‘लाइट ऑफ एशिया’ के अनुवाद ‘बुद्धचरित’ की भी। इस दृष्टि से ‘गोदान’ के अंग्रेजी अनुवाद पर उनका जो विश्लेषण है उसमें डिस्कोर्स, शैली, समाज सांस्कृतिक पक्ष और लोकजीवन को तो केंद्र में रखा ही गया है; इस बहाने उन्होंने ‘साहित्यिक कृति भाषाबद्ध होती है’ इस कथन को भी बड़ी सहजता से हमारे सामने खोल दिया है। इस अध्ययन का प्रारंभिक हिस्सा अत्यंत विचारपुष्ट है जिसमें अनुवाद की चुनौतियों, अनुवादनीयता तथा अनुवाद समीक्षा/मूल्यांकन की तकनीक पर प्रो. सिंह ने अनूठा विमर्श किया है। इसका मूल्यांकन वाला पक्ष भी अत्यंत स्पष्ट और यह जतानेवाला है कि अनूदित पाठ की सीमाएँ लक्ष्य भाषा की सीमाएँ नहीं होतीं वे अनुवादक की सीमाएँ होती हैं।
अनुवाद विज्ञान को सामयिक संदर्भ देने का काम भी प्रो. सिंह ने बखूबी किया है। यह काम वे अपने लेखन में ही नहीं बल्कि संगोष्ठियाँ आयोजित करके, स्मारिकाएँ प्रकाशित करके भी एक लंबे अरसे से करते रहे हैं। उनके सुदीर्घ अनुभव और सतत वैचारिक मंथन से ही यह संभव हुआ कि साहित्येतर अनुवाद की इतनी व्यापक और संपूर्ण पीठिका हमारे सामने आ सकी। इस संदर्भ में उन्होंने साहित्येतर पाठ की अनुवाद समीक्षा का भी प्रारूप हमें दिया है। उल्लेखनीय है कि अनुवाद समीक्षा में भी वे संप्रेषण की भूमिका को भुलाते नहीं। इसके कारण ही उन्होंने व्यावसायिक अनुवाद तथा संचार क्रांति में अनुवाद की भूमिका जैसे अछूते विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई और अत्यंत उपयोगी संकेत हमें दिए हैं जिनके आधार पर हम इन दोनों ही दिशाओं में भारतीय भाषाओं की अनुवादनीय संभावनाओं और चाहें तो उनकी समस्याओं की भी परख कर सकते है। हिंदी पत्रकारिता की भाषा में अनुवाद को देखने के महत्वपूर्ण सूत्र भी वे हमारे सामने रख चुके हैं ; जरूरत इन्हें दिशा देने की है। बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता प्रो. सिंह की वैचारिकता का आधार रहे हैं। संभवतः इसीलिए उनका समाजभाषावैज्ञानिक भी, उनका शैलीवैज्ञानिक भी और साथ ही उनके भीतर का अनुवाद चिंतक भी चयन और संयोजन या एक ही शब्द में कहें तो समायोजन को जिस प्रकार देख पाता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यह भी कह दिया जाए कि अनुवाद विज्ञान की सैद्धांतिकी में निविष्ट उन बिंदुओं में प्रो. सिंह की विषेष रुचि है जो स्रोत भाषा के संस्कारों को लक्ष्यभाषा के भीतर समाविष्ट करने की एक प्रक्रिया है, एक जरिया है और उनकी दृष्टि में यही संभवतः अनुवादक और अनुवाद कार्य दोनों का लक्ष्य है; और यदि नहीं है तो होना चाहिए।
भाषाविज्ञान/ हिंदी भाषा
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की सभी शाखाओं में पैठ रखने के साथ ही प्रो. दिलीप सिंह विवरणात्मक अथवा संरचनात्मक भाषाविज्ञान के भी सजग अध्येता हैं। उनकी यह पकड़ उनके पीछे उल्लिखित अवदानों से भी साफ झलकती है क्योंकि यह तो मानी हुई बात है कि जो व्यक्ति शुद्ध भाषविज्ञान में दीक्षित नहीं होगा वह उसकी सैद्धांतिकी का अनुप्रयोग कर पाने में भी समर्थ न हो सकेगा। भाषावैज्ञानिक परंपरा और उसके विकास के मद्देनज़र ही उन्होंने हिंदी भाषा को देखने का सर्वथा एक नया दृष्टिकोण हमें दिया। इस प्रकार के उनके लेखन से यह स्पष्ट भान हो जाता है कि वे न तो भाषाविज्ञान की रूढ़ियों का अनुकरण करने के पक्ष में हैं और न ही हिंदी भाषा को संस्कृत से अपभ्रंष और फिर खड़ीबोली आंदोलन से जोड़ते हुए उन्हीं-उन्हीं बातों को फिर-फिर दुहराने के, जो ‘हिंदी भाषा संरचना’ अथवा ‘हिंदी भाषा का इतिहास’ के नाम से अनेकानेक बार छापी जा चुकी हैं।
भाषाविज्ञान को उन्होंने एक प्रगतिगामी शास्त्र के रूप में स्वीकारा और प्रतिपादित किया है। इसीलिए वे अपने भाषावैज्ञानिक लेखन में भाषा प्रयोग की दिशाओं का संकेत करते हैं जिसमें उनकी दृष्टि भाषा संरचना और भाषा व्यवहार के परस्पर संबंधों से भाषाविज्ञान के उस ढांचे पर टिकी हुई है जिसे वे भाषा प्रयोग की दिशाओं में देखते हैं। यह उनका वैशिष्ट्य है कि भाषा संरचना के वास्तविक प्रयोग की सरणियाँ उन्होंने इस तरह तैयार की हैं कि भाषाविज्ञान का वह आधुनिक स्वरूप हमें दिखाई दे सका है जो इसके पहले दिखाई नहीं दिया था। बहुभाषिकता तथा कोडमिश्रण/ परिवर्तन की प्रक्रिया में भाषावैज्ञानिक चिंतनधारा उन्हें रुची है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने भाषावैज्ञानिक इकाइयों के ध्वन्यात्मक से लेकर वाक्यात्मक अवमिश्रणों को विश्लेषित कर दिखाया है। कहना न होगा कि इस भाषावैज्ञानिक विचार विमर्श में वे हिंदी भाषा को साथ लेकर चलना नहीं भूले हैं। यह देखा गया है कि भाषाविज्ञान पर बात करते समय सिद्धांत हावी हो जाते हैं। लेकिन प्रो. सिंह ने सिद्धांतों को महत्व देते हुए भी भाषाविज्ञान की उस सामयिक पृष्ठभूमि को महत्व दिया है जिसके कारण परंपरागत भाषाविज्ञान की अवधारणाएँ अब चुकी हुई मालूम पड़ने लगी हैं। इस संदर्भ में भाषिक इकाइयों के मानकीकरण के हवाले से भी उन्होंने भाषाविज्ञान का एक नया पाठ रचा है। इस विचार के अंतर्गत ही उनका यह मानना है कि मानक रूप समाज में प्रचलित अन्य रूपों में से एक विकल्प मात्र होता है। मानक मान लेने भी से अवमानक अथवा अमानक संरचनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता। अतः भाषावैज्ञानिक अध्ययन में अब इन्हें भी सही जगह देने की जरूरत है। इसी धरातल पर भाषानियोजन के प्रश्न को भी प्रो. सिंह ने इस तरह देखा है कि यहाँ व्याकरणिक शुद्धता (जिसे कि अभी भी भाषा नियोजन का प्रमुख मुद्दा माना जाता है) की जगह पर भाषा समुदाय और उसके लोगों की प्रतिक्रिया को प्रमुख माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रो. सिंह उस आगे के भाषाविज्ञान के साथ हैं जो भाषा समुदाय और भाषा समूहों की मान्यताओं को जगह देता है। भाषा नियोजन में उनके चिंतन की धुरी फिशमैन रहे हैं इसीलिए फिशमैन के बहाने उन्होंने व्याकरण की समस्त इकाइयों, शब्द भेदों, ध्वन्यात्मक भेदों, वर्तनी संशोधन तथा पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की बात उठाई है जो परंपरागत भाषाविज्ञान के आमने-सामने रखकर देखने से अलग तो लगती ही है, यह भी पता देती है कि अब भाषाविज्ञान को विवरणात्मक ही न रहने देकर उस विवरणात्मकता को समय और समाज सापेक्ष बनाना जरूरी होगा।
भाषा नियोजन में पहली बार प्रो. सिंह ने उन संभावित संविन्यासों की चर्चा की है जहाँ भाषा का व्याकरण केवल इकाइयों में बँटा नहीं होता, उसकी परख उपरूपों के संदर्भ में की जाती है। उपरूपों की चर्चा से भी आगे बढ़कर प्रो. सिंह सूक्ष्म भाषाविज्ञान और प्रोक्तिविज्ञान तक का सफर तय करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक भाषाविज्ञान की उन अवधारणाओं को वे आज की किसी भी जीवंत भाषा के भाषावैज्ञानिक विश्लेषण में प्रतिफलित होते देखना चाहते हैं जो वास्तव में भाषा संरचना का इकाईगत विवरण न होकर इनकी प्रकार्यता (फंकक्षनलिटी) को उजागर कर सके। इस ओर भी संकेत कर देना जरूरी है कि अपने भाषावैज्ञानिक चिंतन में प्रो. सिंह ने हिंदी भाषा को अथवा कहें उसकी संरचनात्मक इकाइयों को ही सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया है।
हिंदी भाषा की शक्ति को अथवा उसकी समृद्ध परंपरा को प्रकट करने की प्रो. सिंह की प्रणाली एकदम अलहदा है। वे शब्दों की बात करते हैं जिसमें शब्दविज्ञान की समस्त अवधारणाएँ आ मिली हैं तो वे केंद्र में रखते हैं डॉ. रघुवीर को। यह चर्चा वास्तव में डॉ. रघुवीर के बहाने हिंदी शब्दशास्त्र पर है। हिंदी व्याकरण पर भी उनका दृष्टिकोण कुछ ऐसा ही है। उन्होंने शुरू किया है हिंदी के व्याकरणों के परिचय से, और फिर इन व्याकरणों की कोटियाँ तैयार की हैं जो हिंदी के शैक्षिक व्याकरण पर पहुँच कर पूरी होती हैं। उनका यह विवेचन वास्तव में हिंदी का संक्षिप्त व्याकरणी भी है और इस ओर संकेत भी कि यदि आज हिंदी का कोई व्याकरण तैयार करना हो तो उसके अनिवार्य मुद्दे कौन कौन से होंगे। हिंदी के ढेरों व्याकरण हमें मिल जाते हैं लेकिन उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को समेटते हुए इस तरह का आकलन मिलना मुश्किल है।
प्रो. सिंह ने देवनागरी लिपि पर भी लिखा है, दक्खिनी हिंदी पर भी और हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों पर भी। हिंदी भाषा के संदर्भ में ये तीनों पक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इनमें भी प्रो. सिंह ने अपनी उस दृष्टि को सुरक्षित रखा है कि यह केवल चर्चा भर न बने बल्कि इनके भीतर से कभी हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता प्रकट हो, कभी उसकी क्षेत्रगत व्यापकता तो कभी आधुनिकता; और इन बातों को वे बार-बार रेखांकित भी करते चलते हैं ताकि हिंदी भाषा का वह सशक्त ढांचा नितांत भाषावैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सके जो वास्तव में हिंदी भाषा की प्राणशक्ति है। हिंदी, उर्दू, प्रयोजनमूलक हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर की गई उनकी टिप्पणियाँ आधुनिक भाषाविज्ञान की अवधारणाओं से पुष्ट हैं। ऐसा करने से विषय सिर्फ विचार बनकर नहीं रह जाते बल्कि इनके माध्यम से हिंदी का वह सामाजिक यथार्थ भी फूटफूटकर बाहर निकलता है जिसे निकाल कर प्रवाहित करना ही उनका लक्ष्य भी रहा है।
प्रयोजनमूलक भाषा एक लंबे अरसे से अकादमिक बहस का विषय रही है। अभी भी इसके बारे में सोच विचार की सही लीक नहीं बन पाई है। प्रो. सिंह ने प्रयोजनमूलक हिंदी पर विस्तीर्ण चर्चा की है। प्रयोजनमूलक भाषा, उस पर चर्चा के इतिहास और इससे संबंधित देश विदेश की चिंतनधारा को समेट कर उन्होंने उन सारी अनर्गल बहसों को विराम दिया है जो अभी तक घटाटोप की तरह छाई हुई थीं। हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियों पर उनका जो कार्य है वह अतुलनीय है अर्थात ऐसा करके वे कई कदम आगे बढ़ गए हैं। व्यावसायिक हिंदी, पत्रकारिता की हिंदी, साहित्य समीक्षा की हिंदी और यहाँ तक कि पाक विधि की हिंदी के स्वरूप और संरचनागत वैशिष्ट्य का जिस तरह उन्होंने आकलन और विश्लेषण किया है उसे निःसंकोच होकर हिंदी की प्रयोजनमूलक शैलियों के आगामी अध्ययनों के लिए पद्धतियों अथवा प्रविधियों का पुंज माना जा सकता है।
हिंदी भाषा पर बात करते समय जैसा कि उनके जैसे भाषाविद के लिए स्वाभाविक है, उन्होंने हिंदी के सर्वदेशीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों की भी खोज खबर ली है। यहाँ भी वे आकलन मात्र से संतोष नहीं करते बल्कि उन्हें भाषिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में उजागर करते हैं और यह दिखाने का यत्न करते हैं कि हिंदी भाषा का व्याकरणिक, व्यावहारिक और साहित्यिक स्वरूप इतना सघन और फिर भी सहज है कि उसकी व्याप्ति में किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदी भाषा प्रो. सिंह के लिए एक ऐसी भाषा है जो एक भाषा के रूप में ही नहीं, भारत की अस्मिता के रूप में पहचानी और स्वीकार की जाती है।
प्रो. दिलीप सिंह का भाषावैज्ञानिक संश्लिष्ट है। उसके भीतर भाषाविज्ञान की पूरी परंपरा पिरोई हुई है। वह भाषा को सिर्फ एक व्यवस्था मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि इससे अधिक आवश्यक यह है कि भाषा को उसके प्रकार्य, उसकी संप्रेषणीयता, उसकी परिवर्तनशीलता, उसकी अभिव्यंजनात्मक बहुरूपता और उसकी सामाजिकता के संदर्भ में देखा जाए। इसीलिए वे भाषाविज्ञान की उन अवधारणाओं को फलीभूत करना चाहते हैं जिनसे भाषा अध्ययन का ही नहीं, भाषा अस्तित्व का भी पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। प्रो. दिलीप सिंह का एक अवदान यह भी है कि उन्होंने भाषावैज्ञानिक लेखन की एक संप्रेषणीय परंपरा कायम की है। यह उनकी विचार प्रक्रिया की भी विशेषता है और उनके संपूर्ण लेखन की भी।-------------------
- प्रो. ऋषभदेव शर्मा
[पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा], # 208 ए - सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, गणेश नगर, रामंतापुर, हैदराबाद – 500013, ईमेल : rishabhadeosharma@yahoo.com
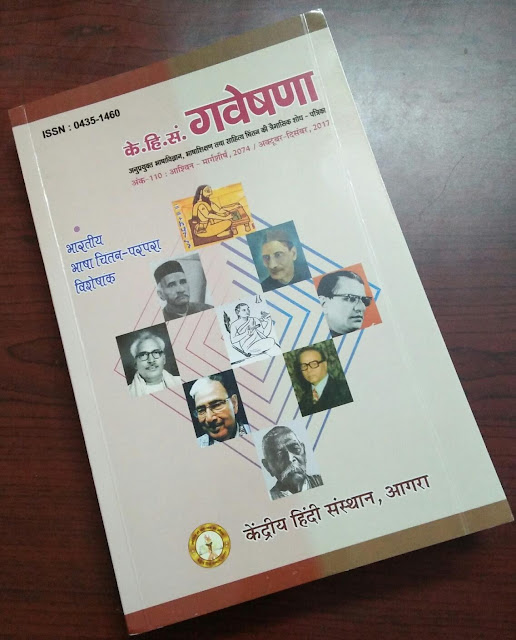
4 टिप्पणियां:
Shukariya bhut acha blog hai ap ka
ipl season 13 winner prediction
ipl toss bhavishyavani 2020
today ipl match astrology
Today Match IPL Bhavishyavani
today ipl match prediction
today ipl match astrology
today ipl match astrology 2020
ipl toss astrology
today ipl match toss astrology
who will win today ipl toss astrology
IPL Toss Astrology
thanks for providing such a great article, this article very helps full for me, a lot of thanks
online education management system
learning management solutions
Hi! I really like your contentYour post is really informative. .
online practice platform for neet
Selena Gomez
Kim Kardashian
Rings Of Power
iPhone 12 Leak Images
Selena Gomez
Avatar 2
Web 3.0
SpacX's Starship
Far Cry VR
Sophia The Robot
एक टिप्पणी भेजें